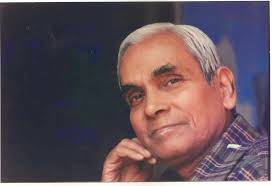
अभाव
किसे खलेगा मेरा अभाव
एक ऐसा पाठ हूँ मैं
जिसे शब्द-स्फीत पाठ्यक्रम से हटा दिया गया
मैं वह स्वतन्त्रता हूँ
ग़ुलामी के दिनों में जिसकी सबको ज़रूरत थी
लेकिन मिलते ही जिसका आशय झुठला दिया गया
वह रचना-बोध
जिसे रचना का स्वाँग रचने वालों ने ही मिटा दिया
फ़ैक्ट्रियों, मिलों और उद्योगपतियों की इमारतों के बीच
किसी झोपड़-पट्टी की ख़ाली ज़मीन हूँ मैं
आपाधापी और महत्त्वाकाँक्षाओं के बीच
मैं वह निःसंग आत्मीयता हूँ
जिसे एक अधूरी पँक्ति-सा बार-बार काटा गया
पर हर बार काटे जाने के साथ
वह परिवेश में कटी हुई अदृश्य उँगलियों-सी आज भी
तैरती है
पॉकेटमार
पॉकेटमार !
भाग्य की पॉकेट मारो
और बाँट दो उसे भाग्यहीनों में
वही तो है तुम्हारा परिवार
जानता हूँ मैं तुम्हारा वर्तमान
तुम्हारा भविष्य
पर बेड़ियों से और हथकड़ियों से डर कर क्या तुम
भाग्यहीनों के आँसुओं के उस रास्ते को
तब्दील करने से मुकर जाओगे
जो उन्हें सिर्फ़ मौत की ओर ढकेलता है
साफ़ कर दो उस परिवेश की जेब
जहाँ विकास नपुंसकता का पर्याय बन जाता है
लोकमत चुनवा दिया जाता है मत-पेटिकाओं में
आरोपों-प्रत्यारोपों से सजी-धजी
ठगती है वेश्या राजनीति
सबूत के अभाव में लड़खड़ाता हुआ
गिरता है किसी उच्च रक्तचाप के रोगी-सा न्याय
निर्दोष की विवश्ता भरी यन्त्रणा से बढ़कर
क्या और कोई जेल हो सकती है
पॉकेटमार !
कविता के बाहर
तुम एक कविता लिखते हो
और एक बिच्छू अपना नुकीला डंक लिए
तुम्हारी ओर दौड़ पड़ता है
तुम दूसरी कविता लिखते हो
और एक सर्प तुम्हारी ओर बढ़ने लगता है
फन काढ़ कर वह तुम्हारे हाथों की ओर झुकता है
तुम तीसरी कविता लिखते हो
और एक भेड़िया तुम्हारी ओर देखकर गुर्राता है
तुम कोशिश करते हो एक और कविता लिखने की
और एक बर्बर समूह तुम्हारी ओर झपट पड़ता है
बेहतर क्या है
आज के समय में कवि होना
या एक बिच्छू, एक साँप, एक भेड़िया
या एक बर्बर समूह बन जाना ?
बताओ, कवि !
बिच्छू, साँप, भेड़िए और बर्बर समूह
तुम्हारी कविताओं के भीतर तो मरते हैं
पर क्यों नहीं मरते तुम्हारी कविताओं के बाहर ?
कवि ! तुम मौन क्यों हो ?
समय के बाहर
समय मुझे
अपने से बाहर फेंक रहा है
ओह !
कैसा होता है
समय के बाहर फेंक दिया जाना ?
समय के बाहर जीना,
समय के बाहर ही
मर जाना ।
कीच सने पाँव
कीच सने पाँव क्या सदा भद्दे ही होते हैं ?
कीच क्या सदा बदबू ही देती है ?
किसने आँका है कीच की शक्ति को ?
कीच सने पाँवों ने नाप डाली है अब तक
जाने कितनी धरती ?
लिपट जाती है गीली-गीली
तो या तो
पाँवों से अलग होते-होते
पानी में भी अपनी छाप छोड़ने लगती है
या पाँवों से लिपटी-लिपटी ही
सूख जाती है
जैसे कोई कुरूप-सती नारी
कीचड़ सने नंगे पाँव दौड़ पड़ते हैं प्रभु
किसी भक्त की गुहार पर
कब तक बचेगी मोज़े की नफ़ासत
कीच सने पाँवों से
जबकी हावी होते जा रहे हैं
किसी सर्वव्यापी की तरह लगातार
कीच सने पाँव ।
रिश्तों की ज़बानें भूल गए
रिश्तों के ज़माने भूल गए
रिश्तों की ज़बानें भूल गए,
मज़हब की उलझी डालों में
अश्कों की ज़बाने भूल गए ।
तहज़ीब की सिलवट याद रही
वो ख़ुलूस की बाहें भूल गए,
क़ुदरत की हँसी वो रुसवाई
सब गूँगे रिश्ते भूल गए ।
ये चेहरा पहचाना है
गली-गली में, डगर-डगर में
भटक रहे सुनसान नयन,
ऐसा क्या वीरान शहर में, जो याराने जैसा है…
बसा अजनबी नज़रों में,
घूर रहा इन्सान यहाँ,
कौन यहाँ है जो पूछे — यह चेहरा पहचाना है?
मेरे इस देश में
मेरे इस देश में आहों के सिवा
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं
कटी बाहों, कटी टाँगों, कटी राहों के सिवा
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं
मेरे इस देश में क़ातिल तो बहुत मिलते हैं
मगर इस देश को सरसब्ज़ बनाने के लिए
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं
बड़ी उम्मीद, बड़ी आस, काग़ज़ी तहरीरें
मेरे इस देश में शब्दों के सिवा
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं
जवाब
तुम न दिन की तरह निकले
न फूल की तरह खिले
रजत-रात की तरह किसी दिल में महके भी नहीं
क्या जवाब है तुम्हारी आत्मा में उनके लिए
जो दिन का इन्तज़ार कर रहे हैं
फूल के खिलने की बाट जोह रहे हैं
रजत-रात की धड़कनों को
मुरदा-दिलों में सुनने को बेचैन हैं
पर जो दब गए हैं भरी-जेबों के अन्धेरों में ।
निर्वासन
देश में होकर भी
निर्वासित हूँ
(देता हूँ दिलासा अपने को)
निर्वासित होकर भी
देश में तो हूँ…।
दीवार
अब तबियत कैसी है ?
किसी ने पूछा
उस ढही दीवार से
वह बेचारी क्या बोलती
मौन
नज़रें झुकाए
सीलन-भरे सिकुड़े होंठों से वह मुस्कराई ।
देश के
सारे बुलडोजर
ख़ुशी के मारे
अपने को क्रान्तिकारी समझ
नाचने लगे ।
बदले पैमाने
गोली लगी
झुकी हुई पीठ में
निकल पड़े ख़ून की जगह
घुन लगे गेहूँ के दाने
सभी थे भूखे
बाँट लिया मिल-जुल
सिपाहियों ने
हत्यारों ने
भ्रष्ट मुकुटों ने
मौसम तो यह भाईचारा देख दंग रह गया
चिड़ियों की चोंचों से छूट गए गाने
काँपे गुफ़ा-घाटी,
बदले पैमाने
बिना रटे सबक बच्चे हो गए सयाने ।
धीरे-धीरे
चली मिनिस्ट्री धीरे-धीरे
बढ़े गिरहकट धीरे-धीरे
सड़कें धँसतीं धीरे-धीरे
ईंट खिसकती धीरे-धीरे
झाड़ा प्लास्टर धीरे-धीरे
गिना बहत्तर धीरे-धीरे
बीत गए दिन, बीती रातें
बीत गए तुम धीरे-धीरे
रचना
सूर्य उदित हुआ
किसी बहुत बड़े नीले दोने में रखी हुई जलेबी
कृषकाय भूखी गर्भिणी प्रतिमा
किसी मरियल कुतिया-सी
उसकी ओर लपकी
और फिर इतनी मार खाई
कि रचना गर्भ में ही मर गई।
नसीब लोकतंत्र का
कीलें बिल्कुल ठीक जड़ी गई हैं
एक कील मेरे सिर के बीचोंबीच जड़ी गई है
दो कीलें मेरी आँखों में
दो कीलें मेरी दोनों हथेलियों में
मेरे पीछे एक चिकना सलीब
मेरे पैरों में दो कीलें ठुकी हुई हैं
समझ में नहीं आता
कि मेरी जीभ में कील क्यों नहीं ठोंकी गई
लोकतन्त्र का नसीब
क्या धँसी हुई कीलों के बीच जीता है?
संवेदना के सीमान्तों में
फटा हुआ
(किसी-के कलेजे-सा)
तो मैं था ही
जिसे किसी ने लेई लगाकर जोड़ दिया था
ऎसा चिपकाया था
कि हल्का-सा पानी या थूक लगने से भी खुल सकता था
जैसे-तैसे
मैं पहुँच ही गया था तुम्हारे पास तक
तुमने अपने सिले होंठों से मुझे खोला
और मैं खुल गया पूरा का पूरा
तुमने पत्र-सा मुझे पढ़ा
फिर उसी तरह मोड़ कर रख दिया
किताबों के ढेर के बीच
मैं फिर से खो गया
तुम्हारी संवेदना के सीमान्तों में
मेरे पाठक!
सितारे साम्राज्यवादी नहीं होते
सितारे साम्राज्यवादी नहीं होते
वे चमकते हैं शिशुओं के हृदय और आँखों में
वे प्रतीक्षा करते हैं उनके जवान होने की
और फिर आहिस्ता से उन्हें मुक्त कर देते हैं
उनके मनचाहे स्वप्नों के लिए
वे जहाँ रात देखते हैं
वहीं चमकने लगते हैं
सूरज की भूमिका समाप्त होने के साथ ही
उनकी भूमिका शुरु हो जाती है
वे सारी रात चमकते रहते हैं
अगले सूर्योदय की प्रतीक्षा में
दुनिया से बेदख़ल होती मानवता को
वे आमन्त्रित करते हैं अपने अन्तःकक्ष में
विचारित नहीं होते वे वैज्ञानिकों और ज्योतिषियों के गणित से
वे मुस्कराते हैं कलाकार के रंगों में
संगीतज्ञ की मीड और गमक में
सितारे साम्राज्यवादी नहीं होते
वे बेचैन रहते हैं नाकाम करने को
कुटिलताओं और साज़िश भरे मन्तव्यों को
लेकिन एक उल्कापात होता है
तब कोई मर जाता है बेसहारा
और वंचित रह जाते हैं सितारे
उसके प्राणों की रोशनी बन पाने से ।
फ़्रेम के दो पहलू
हम तुम
फ़्रेम के दो पहलू !
हमारे-तुम्हारे सहारे ही
सत्य की यह तस्वीर खड़ी है !
पर देखो,
यह कितने आश्चर्य की बात है —
कि समय ने मुझ पर
अपनी सारी कीलें जड़ दीं
जब कि
तुम पर
फूल दही अक्षत है
बालक
वह एकान्त
बर्फ़ की ताबीज औ’ गण्डे लपेटे
बुद्धू-सा खड़ा था चुपचाप मैं
एक बादल कहीं से आया
बिना किसी बात मुझसे टकरा गया,
और स्वयं ही फूट-फूट रोने लगा
हवा मुझे चपत मार कर भाग गयी
मैं कुछ नहीं बोला
खीझा, घबराया सा खड़ा रहा
सहसा ध्यान गया
मैं नंगा था -–
लजाया सा इधर-उधर देखा
बादल भी गायब था
लगा, कहीं वह किसी से कुछ कह न दे
पर जब समूर की खाल ओढ़े
सतरंगी घड़ी लिए सूर्य निकट आया
मैंने नीचे पड़ी
वह फूलदार घाटी पहन ली थी