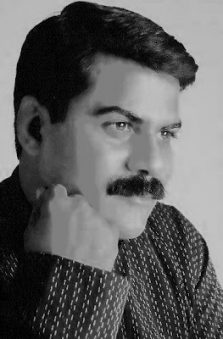 अभिधा की एक शाम नरबलि
अभिधा की एक शाम नरबलि
एक छोटी शाम जो
लम्बी खिंचती जाती थी
बिल्कुल अभिधा में।
रक्ताभा लिए रवि
लुकता जाता था।
लक्षणा के लद चुके
दिनों के बाद
अभिधा की एक छोटी-सी शाम
धीरे-धीरे
करती रही अपना प्रसार
बढ़ती जाती थी भीड़
सिकुड़ता रहा सभागार।
रचना ही बचना है
कोहराम मचना है-
कहा कभी किसी ने
बे दांत जबड़ों के बीच
कुतरे जाते हुए।
अहंकार से लथपथ
शतपथी ब्राह्मणों के
पान से ललाये मुख
से होते हुए आखिर
पेट में जा पचना है।
आयताकार प्रकाश पुंज
फैला है भीतर
बाहर शाम को
लील रहा अंधकार
मंच पर आसीन
पहने कौपीन
लकदक लिये घातक हथियार
आतुर थे करने को एकल संहार।
वायु-मार्ग से आये
ऋषिगण करते आलोचन
लोहित लोचन।
थके चरण वह वधस्थल
को जाता उन्मन नतनयन।
माला और दुशाला को
डाला एक कोने में;
वध के पश्चात् रक्त
सहेज कर भगोने में,
तेज़ धार वह कटार
पोंछ-पाछ साफ़ कर
अन्तिम यह वाक्य कहा-
“हल्का है, बासी है कल का है,
डिम्ब है न बिम्ब है
अभिधा है, अभिधा है
अग्नि को जो अर्पण है
मेरी प्रिय समिधा है।”
आदिवासिनी
मैं जंगली लड़की हूँ
तुम लोगों की
कब्जे़ की लड़ाई में
बार-बार मात खाती हुई ।
सबका मालिक एक-
है आज भी
अपनी सारी अर्थच्छवियों में।
जब उस एक के खिलाफ़
हम सम्मिलित खड़े होते हैं
तो तुम हमें नक्सली कहते हो।
तुम एकल न्याय के नाम पर
सामूहिक नरसंहार करते हो।
तुम्हें हमारे जंगल चाहिए
तुम्हें हमारी ज़मीन चाहिए
तुम अपनी सभ्य भाषा में
हमारे शरीर का ही अनुवाद करते हो
चाहे वह जीवित हो या मृत।
अपनी सभ्यता में
हमारी कला, हमारी संस्कृति,
हमारी देह और हमारे देश पर
कब्ज़ा करने वालों से
मैं कहती हूँ –
“जान देबो, ज़मीन देबो ना”
नफ़रत की तमीज़ को
अपनी बोली से
तुम्हारी भाषा में रूपान्तरित करते हुए।
ईश्वर
(अपने गुरू सत्यप्रकाश मिश्र के लिए)
लोग उसे ईश्वर कहते थे ।
वह सर्वशक्तिमान हो सकता था
झूठा और मक्कार
मूक को वाचाल करने वाला
पुराण-प्रसिद्ध, प्राचीन।
वह अगम, अगोचर और अचूक
एक निश्छ्ल और निर्मल हँसी को
ख़तरनाक चुप्पी में बद्ल सकता है।
मैं घॄणा करता हूँ
जो फटकार कर सच बोलने
वाली आवाज़ घोंट देता है।
ऎसी वाहियात सत्ता को
अभी मैं लत्ता करता हूँ।
उस स्त्री के भीतर की स्त्री के बारे में
उस स्त्री के भीतर
एक घना जंगल था
जिसे काटा – उजाड़ा जाना तय था
उस स्त्री के भीतर
एक समूचा पर्वत था
जिसे समतल
कर दिया जाना था
उस स्त्री के भीतर
एक नदी थी
बाढ़ की अनन्त
संभावनाओं वाली
जिसे बांध दिया जाना था
उस स्त्री के भीतर
एक दूसरी देह थी
जिसे यातना देते हुए
क्षत -विक्षत किया जाना था
किन्तु उस स्त्री के भीतर
एक और स्त्री थी
जिसका कोई कुछ
नहीं बिगाड़ सकता था
क्या फर्क पड़ता है
क्या फर्क पड़ता है
एक आदमी अपने चार बीघा
खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत
के बाद हासिल कर्ज़ अपने झोले में
सहेजे आत्मघात की तरफ
चला जा रहा है।
एक औरत अपने लम्बे
विश्वास से बाहर
लुटती-पिटती लौट रही है
भीतर के दुःखों को सम्हालती।
एक बच्चा जो
कूड़े में खेल रहा था
बम फटने से मारा जाता है
जेब में तीन चिकने पत्थर लिए।
एक लड़की जो
दुनिया में आने की सज़ा
पाती है और नीले निशान
अपनी फिरोजी फ्रॉक से छिपाती फिरती है।
क्या फर्क पड़ता है!
हमारे समय का बीज वाक्य है
यह हमारे समय का
अन्तिम सत्य
किसी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता
तमाम गाजे-बाजे और
इक्कीस तोपों की सलामी से
हमें भी क्या फर्क़ पड़ता है।
चार पुरुष और स्वर्ण युगों पर शोकगीत-1
हम चार दोस्त थे,
बिल्कुल आवारा, लेकिन
सँस्कृति के प्रश्नों को
अपने कन्धे पर उठाए
सँस्कृतिकर्मी कहलाने को उत्सुक।
हम अपने इतिहास को
लेकर सिर धुनते
हम जीवन के ठाठ अनश्वर
बिनते-चुनते ।
हम प्रश्नाकुल
दीवारों पर जगह-जगह
प्रश्नचिन्ह टाँगें
हम भोले बचपन-से
अपने-अपने उत्तर माँगें ।
सत्ता के गलियारों की
आपा-धापी में
अक्सर वन्दन अभिनन्दन
कीर्तन-भजन-पूजन ।
हम निर्जन में जैसे बन्दी
बहुत अकेले
पाँवों में चलने की सूजन ।
परम विकट पथ चुना हुआ
अपना ही था
यह थकान-सुस्ती-ढीलापन
अपना ही था
रेशे-रेशे बिखरा जीवन
अपना ही था ।
सन्नाटे में
प्रश्न-उत्तरों की उधेड़बुन
सभी शास्त्र-ग्रन्थों को पढ़-गुन
आगे बढ़ते अपनी ही धुन ।
यूँ तो संगी विरले मिलते हैं
फिर भी दोस्त बने थे चारों
कवि, क़िस्सा-गो
इतिहासकार और ख़बरनवीस ।
क़िस्सा-गो, वह प्रथम पुरुष
बेलगाम घोड़ों पर
हर समय सवार
किधर जाएगा, किसे ख़बर ?
उसके हाथों में काठ की
दो तलवारें हैं
माथे पर दुश्चिन्ताओं
की सतरें हैं
ख़ुद कहता है — शापित है
उसने भी मुट्ठी तानी थी
दुर्वासा के शाप से इतना थर्राया
अब एड़ियाँ घिसा करता है ।
फूट रहा है कोढ़
इसलिए अँगौछा ओढ़
चिड़ीमार-सा
परिन्दे पकड़ता है, उड़ता है
अकेले में कुनमुनाता है
रोज़ एक नया क़िस्सा सुनाता है ।
द्वितीय पुरुष —
वह कवि जिसने
आस्तीन में साँप की तरह
आँखों में सपने पाले हैं
उनमें से कुछ को ही
सच होते देखा ।
कुछ सपने नाकामी के
कुछ भयावने
कुछ सपने
सपने तो क्या, गड़बड़झाले हैं ।
फिर भी नाउम्मीद नहीं है
उम्मीदों की फ़सल काटकर
अपनी ख़ाली जेबों को भर
वह आगे बढ़ता जाता है ।
अपने समय के जितना भीतर
उतना बाहर
वह वामन अपने छोटे क़दमों से ही
युग-युग को नापा करता है ।
छन्दों को तोड़ता-जोड़ता
जीवन की लय
पकड़ता-छोड़ता
प्रियवाची काव्य-पुरुष ।
तृतीय पुरुष —
इतिहासकार वह स्वतन्त्र ।
बहुत अहिंसक
युगों-युगों की राख कुरेदता
सत्य-शोधक ।
उसका जीवन अभिशप्त शिला
जिस पर नहीं लिखा गया
कोई लेख
कद-काठी का
गर्वोन्नत विजय-स्तम्भ ।
साम्राज्यों के उत्थान-पतन
की बातें करता
राज-व्यवस्थाओं का
वह विश्लेषक
अपनी झोली में
जब भी हाथ डालता है
एक नायाब चीज़ निकालता है ।
काले-लाल-धूसर मृदभाण्ड
सोने, चाँदी, चमड़े के सिक्के
कटी-फटी प्रतिमा
अथवा अन्नादि के जले हुए कण ।
अपने औजारों से वह
हथियारों को परखा करता
लिए हुए एक सन्दूकची
चलता-फिरता
सभ्यता का सांस्कृतिक अजायबघर ।
चौथा पुरुष — पत्रकार
स्कूप तलाशता
दौड़ता-भागता
सम्पादकों पर लानतें भेजता
मालिक को गरियाता ।
चोरी-डाका-दुराचार
थाना-कचहरी-तहसीलदार
सबको साधते पस्त
लोकतन्त्र का चौथा पाया ।
अपने समाज का वह प्रहरी
समझा करता है
सत्ता की
सब चालें गहरी ।
पूर्वजन्म के नारदोचित
सँस्कारों से
जगह पर, समय पर उपस्थित ।
चार पुरुष और स्वर्ण युगों पर शोकगीत-2
हम थे चार पुरुष
आपस में लड़ते-झगड़ते
स्वर्णयुग का हर यूटोपिया
हमको आकर्षित करता था ।
कुत्ते की तरह हाँफते हुए
हम उस तक
किसी भी सूरत में
पहुँच जाना चाहते थे ।
बदहाल, लगभग मनुष्य विरोधी
स्थितियों में
अपने जीवन को झेलते
अपने एक जैसे जीवन को काटते ।
हमने अपने को ही खाकर
भूख मिटाई
हमने अपना लहू चाटकर
प्यास बुझाई
ख़ुद को समिधा मानकर
हमने आहुति दी
तिल-तिल
देह गलाते गए
अन्तस् को जलाते गए ।
हमने तक़लीफों को छूकर
महसूस किया
पीड़ा को सीने में धरकर
समझा है
जो कुछ भी देखा और जाना
जितने अंशो तक
हमने सत्य को पहचाना
उतने तक
वैसा कहने के खतरे उठाए ।
अपने समय को
नपुंसक कहकर
हम किसी स्वर्णयुग की
जालिम कल्पना में तल्लीन थे ।
अपने सीमित और भोंथरे
हथियारों पर
हम बहुत गर्व करते थे ।
हम लड़ाकू थे
एकदम मौलिक
विचारों की लड़ाई में
समान रूप से निपुण
हम चारों
पीठ पीछे वार नहीं करते थे
हम प्रतिपक्ष को
पूरा मौक़ा देते थे,
इसलिए अपने को नैतिक कहना
हमें अधिकार की तरह लगता था ।
हम विचार को
विचार से परास्त करना
चाहते हुए भी
बार-बार ख़ुद हार जाते थे
क्योंकि प्रतिपक्ष
विचारों की लड़ाई को
अपने कूड़ेदान से शुरू करता था
और चाकू पर
लाकर ख़त्म कर देता था ।
दरअसल
मायावी था हमारा शत्रु
वह नए रूप धरता जाता था
और उसकी शिनाख़्त मुश्किल थी ।
अपने सबसे अच्छे समय
के हम लोभी
मरुस्थल में गिरते-पड़ते
कितनी ही आँखों में गड़ते
हर सूर्योदय के बाद
जब हम निकलते
तो यह सोचकर कि लेकर
आएँगे कोई न कोई स्वर्णकाल
या तो मौत हमें वापस
एक साथ मिलने नहीं देगी ।
इस तरह हमने
उन तमाम लोगों को बेवज़ह
डरा दिया था
जे हमें कुछ दिन और
जीवित देखना चाहते थे ।
वे लोग
अपने अच्छे दिनों के
न आने से खीझे हुए
पोलियो के कारण
दोनों पाँव की ताक़त खोए
रोगी की तरह
अपने हाथों में
हवाई चप्पलों के साथ
घिसट रहे थे ।
बेहद छरे हुए खभ्भड़
वे सिर्फ़
इस देश का नागरिक
बने रहने की
जद्दोजहद कर रहे थे ।
वे एक अदद
मतदाता पहचान-पत्र
हासिल करने के लिए
बार-बार फोटो खिंचा रहे थे
परन्तु हर बार उनकी मानवाकृति
बैल में बदल जाती थी ।
वे सब
हमारे ही प्रियजन थे
और हमारा
अवांछित भविष्य हो सकते थे ।
कुछ लोग बिल्कुल चुप थे
जिन्होंने कई बार
नाजुक मौकों पर हमें
आत्महत्या का परामर्श दिया
वे सब आत्म-वध को भी
क्रान्ति मान चुके लोग थे ।
हमसे पहले भी आए थे
सब सच-सच कहने वाले
दुनिया को अपना
शोधा सच बतलाने वाले
दुःख है तो
दुःख का कारण समझाने वाले
समतल धरती को
गोल-गोल दिखलाने वाले ।
चार पुरुष और स्वर्ण युगों पर शोकगीत-3
वसन्त की पहली सुबह
जब हम जागे
हमें सामने खड़ा मिला
एक दिव्य पुरुष ।
ऐसा जिसे देखते ही
उमड़ पड़े श्रद्धा ।
उसकी लाल-लाल आँखों
के भीतर एक साथ
चारों ने झाँका
और किसी सम्मोहन में
बँधकर बैठ गए
अपने से वँचित ।
उसने हमसे कुछ भी न कहा
इस तरह हमारे साथ रहा
उतने समय में भीतर-बाहर
कि हम आतँकित होने लगे थे ।
उसका होना
एक तड़प का होना था
एक छटपटाहट
उसके साथ चली आई थी
हमारे भीतर
इसीलिए भय था ।
हम चाहते थे कि बने रहें
हम जैसे हैं, वैसे ही
तो क्या हर्ज़ है ?
लेकिन, वह न तो हमें
और न दुनिया को
इस तरह देख सकता था ।
वह मौन में भी
सिर चढ़ कर बोलता जैसे
वह बोलता तो
श्रोता बेचैन हो उठते
वह अदृश्य होता
तो और गहरा जाता उसका एहसास ।
वह महात्मा नहीं
ज्ञानी नहीं वह
नास्तिक नहीं
अभिमानी नहीं
कोई नजूमी नहीं, वह प्रियंवद ।
वह चाहता था
कि हम जिएँ उसकी तरह
मगर वैसे हम जी नहीं सकते थे
वह चाहता था
कि हम सोचें उसकी तरह
मगर वैसे हम सोच नहीं सकते थे
वह चाहता था
कि हम हो जाएँ उसकी तरह
मगर हम उसकी तरह
व्याप्त नहीं हो सकते थे ।
अपनी छोटी-छोटी
सीमाओं के हम क़ैदी
उसका कहा नहीं मान पाए अभी ।
हमने हृदय से
उसके अभिनन्दन किए
असहायता की सारी लाचारी के साथ
फिर मिलने के आश्वासन पर
हम चारों
अलग-अलग दिशाओं में चले ।
चार पुरुष और स्वर्ण युगों पर शोकगीत-4
हम चार दोस्त
चार दिशाओं में
बीते कल की डोर पकड़ कर
अतीत के कुण्डों में
डुबकियाँ लगाते
काश ! हाथ आ जाए
कोई स्वर्णयुग ।
प्रथम पुरुष ने
कूच किया सरयू की ओर
क़िस्सा-गो वह
रामराज के क़िस्से में
डूबा-उतराया
कई माह सरयू के तट पर
कभी-कभी
जल भीतर घुस कर
रहा खोजता एक स्वर्णयुग ।
उसे एक स्त्री मिली
स्वर्ण-प्रतिमा में बदली हुई
अपनी माँग में
किसी राजा के नाम का सिन्दूर भरे हुए
उसके दोनों ओर
दो बच्चे थे मरे हुए ।
एक ऋषि मिले
अपने श्वेत केश खुजलाते
और लगभग शाप की तरह
मिली हुई लम्बी उम्र पर पछताते ।
उसे एक हिरणी मिली
किसी राजकुमार की छट्ठी में
सीझे हुए
अपने हिरण की गन्ध से व्याकुल
इधर-उधर भागती,
उसे एक धोबन मिली
सब दाग़ धोती
रात-रात भर रोती-जागती
विगत कल में, सरयू जल में ।
होता तो मिलता
न स्वर्णयुग राम का ।
कनक भवन की परिक्रमा कर
मक़तूल शम्बूकों से डर
सरयम से मुँह मोड़
अपना अंगौछा छोड़ वह भागा ।
सरयू में गोते खाकर
जाना उसने अवध में जाकर
रामराज स्वर्णयुग होता
तो सरयू भर पानी में
क्यों डूब मरते भगवान ?
द्वितीय पुरुष-कवि
चला गया उज्जयिनी
महाकाल के मन्दिर में गिरा
वह जाकर, गश खाकर ।
मालवा के आकाश में
उसने मेघों से होड़ लगाई
भटकता रहा बहुत दिनों तक
कालिदास की उज्जयिनी में
मेघदूत, यक्ष अथवा
विरहिणी प्रिया को
न पाता हुआ कवि
लौटा महाकाल के पास
न वैसी उज्जयिनी
न वैसे चन्द्रगुप्त न कालिदास ।
स्वर्णयुग भी वह क्या भला
जिसमें कोई
सिसकियाँ भर-भर रोता हो
कोई गान भी गाता हो
तो दुःख से फट पड़ते हों मेघ
कोई भीतर-भीतर जलता हो
और बढ़ जाता हो
पूरी पृथ्वी का तापमान ।
बिना किसी तर्क
आगत और विगत का फर्क़
इस सोने का
इस युग का हो बेड़ा गर्क़
हाय कितना विष
कैसा नर्क !
कवि बेहद निराश हुआ
और पहले से ज़्यादा
उम्रदराज़ दिखता हुआ
वहाँ से लौटा ।
अपने सुख और श्री से वंचित
गँवा कर अपना
सब कुछ संचित
भीख माँगते मिले
कवि-कुल-गौरव कालिदास ।
तृतीय पुरुष
उस इतिहासकार ने
मुस्कुराते हुए अग्नि में प्रवेश किया ।
स्वर्णयुग लाने की ख़ातिर
वह ख़ुद गोया कुन्दन बन
जाना चाहता था
यह था पूर्ण समर्पण उसका ।
अग्निद्वार पार कर
पहुँचा यमुना-तट पर
मुग़ल काल में ।
कहाँ गया वह मुगल स्वर्णयुग
ढूँढ़ा फिरा वह
दीन-ए-इलाही
मगर मिली बस उसे तबाही ।
मिले उसे
छोटी-सी कुटिया में
लगभग अज्ञातवास झेलते
मानस पर जमा
धूल की परतें
पोंछ-पांछ कर साफ करते
जर्जर तुलसी ।
विनय पत्रिका का अकाल
इतिहासकार को
पहली बार दीखा ।
पहली बार ही उसने जाना
जैसे मिट्टी की
परतों के नीचे और परत
वैसे ही इतिहास के नीचे
एक और इतिहास ।
कह ही दिया जाता है अकथ्य ।
एक सत्ता के समानान्तर
दूसरी सत्ता
सत्य की, साहित्य की ।
अबुल फजल, अल बरूनी
स्मिथ, हेग, टॉड वगैरह
जब लिखते हैं इतिहास
मुस्कुराते हैं स्वर्णयुग ।
कोई स्वर्णयुग
जब मक़बरे में तब्दील
होता है
तब सिरहाने के पत्थर पर
चीख़ता है झूठा समाधि-लेख ।
हताश इतिहासकार
वह तृतीय पुरुष
सीकरी के
एक लाल पत्थर
पर सिर पटक कर
रोने लगा ।
उड़ चले खून के छींटे
टूट गया विश्वास
उसके फटे हुए सिर के साथ ।
समय के शिलालेख पर
दर्ज हो शायद कभी
एक टूटा हुआ इतिहासकार
और उसके रक्त से
हुआ और गहरा वह लाल पत्थर ।
ख़ून से भीगा
इतिहासकार
डूबते सूर्य की तरह लौटा ।
चौथा पुरुष
लोकतन्त्र का चौथा पाया थामे
हवा को सूँघता
और वायु के साथ ही
पहुँचा नेहरू के युग में ।
आधुनिक भारत के
स्वर्णयुग की तलाश में
टकराया भूल से
किसी की छाती में
गड़े त्रिशूल से ।
छूरों और कटारों से
लुकता-छिपता वह भागा
खुली आँख
स्वर्णयुग ढूँढा
तभी दीखा कोने मे
हे राम ! कहता एक बूढ़ा ।
अचानक दृश्य बदला
और उसने देखा
ख़ून की एक गहरी लकीर
जहाँ बाँट रही थी
इस महादेश को
ठीक वहीं
गोली चली
और मारा गया इतिहास-पुरुष,
अकाल-पुरुष वह वृद्ध ।
उसकी आँखे
कीचड़ से चिपचिपी हो चलीं
उसके नथुनों में
प्राणवायु के साथ
घुसने लगी सड़ रही लाशों की दुर्गन्ध ।
जरायमपेशा लोगों का
पूरा जमघट लगा हुआ था ।
आश्चर्य और सन्ताप
के मिश्रण से
वह भरभरा कर गिर पड़ा ।
खुदाई खिदमतग़ारों की
मदद से किसी तरह
एक रेलवे स्टेशन
पहुँचकर उसने पाया
कि यह शहर चण्डीगढ़ था
और उसका
‘प्रेस-पास’ कहीं गिर चुका था ।
वायु-गमन के बाद
रेल से पहली बार बिना टिकट
यात्रा में
पकड़े जाने के भय से
वह गन्तव्य स्टेशन से पहले ही
आउटर पर
चलती ट्रेन से कूद पड़ा
और अपने हाथ-पाँव तुड़वा बैठा ।
चार पुरुष और स्वर्ण युगों पर शोकगीत-5
हम चार पुरुष
चार दिशाओं में
जल, नभ, अग्नि और वायु
से आत्म-लज्जित
खाली हाथ लौटे हुए
जब मिले
तो एक दूसरे से गले लग-लग
खूब देर तक रोते रहे ।
शिशिर की घोर रात में
काँपते हुए
चार पुरुष हम
उस वसन्त का स्मरण करते
जिसमें मिला था दिव्य-पुरुष ।
यह अन्धेरी रात थी
और हम सब शीत से आतँकित
तभी हमें ईशान कोण से
आता हुआ
जलती हुई मशाल-सा
दीखा वह दिव्य-पुरुष ।
उससे हमने अपने सब
दुखड़े कह डाले
अपना-अपना आँखों देखा
सच बतलाया
हमने अपने घाव दिखाए
अपने भयावह अनुभव
उससे बाँटते-बाँटते
हम चारों
एक बार फिर रो पड़े ।
विलाप और करुणा के बीच
सिगरेट सुलगाते हुए
दिव्य-पुरुष घूमा ।
एक लम्बा कश खींचकर
हमारी ओर पीठ कर
ज़ोर से बोलना शुरू किया उसने
वक्तव्य दे रहा हो मानो
सम्बोधित करते हुए पूरा हिन्दुस्तान–
‘‘किसी स्वर्णयुग के
दमकते हुए सोने की
नक़्क़ाशी के भीतर
अगणित घाव
अनवरत रक्तस्राव ।
सबसे जोख़िम है इतिहास
में उत्खनन ।
सिंहासनों पर
बदलते हैं शासक जैसे-जैसे
सल्तनतें बदलती हैं
वैसे-वैसे निष्ठाएँ
और काल के पत्र पर
सरकारी मुहर के साथ
अँकित हो जाता है
अँगार के समान चमकता एक स्वर्णयुग ।
किसी भी कालखण्ड के
ज़ख़्म कभी नहीं भरते
वक़्त भर भी नहीं सकता
कोई ज़ख़्म
किसी युग के ज़ख़्मों से
रिसता हुआ लहू
इतिहास से ज़्यादा
साहित्य में दाखिल होता है ।
किसे कहते हो स्वर्णयुग —
जिसमें जागता है कवि
रात-रात भर
या वह जिसमें
रातें नागिन-सी डसा करती हैं
वह कौन सा स्वर्णयुग
जिसमें कोई फरियादी
निरन्तर रोने और
कभी भी नींद भर न सोने
की शिकायत करता है ।
कौन वह स्वर्णिम काल
जहाँ दुर्भिक्ष-अकाल
फटता है धरती का कलेजा
एक भूमिजा स्त्री
हार कर फिर
धरती में समा जाती है ।
अथवा समानता की माँग पर
एक दलित
क़त्ल कर दिया जाता हो जिसमें ।
इतिहास से बाहर
एक कविता
क़ैद कर लेती है
इतिहास-पुरुषों के
जूतों तक के निशान ।
इतिहास में सुरक्षित होंगे
अशोक महान् हो कर
वहीं, कहीं आस-पास
समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अकबर
कितने शक, कितने हूण
कनिष्क के साथ कितने कुषाण
मंगोल, चोल, चन्देल
परमार, सिसोदिया और चौहान
लेकिन वह कौन स्वर्णिम अतीत
जब कोई कुचलवा दिया जाता है
उन्मत्त हाथी के पाँवों तले
किसी का हाथ
काट लिया जाता है ।
किस काल में होता है प्लावन
पोत में बचाए जाते हैं
किसी तरह बीज-ज्ञान
कब फटते हैं ज्वालामुखी
भूमि कब होती है कम्पायमान ।
सब कुछ निषिद्ध
होता है किस समय
खत्म हो जाते हैं
सारे अधिकार
शेष रह जाते हैं बस कर्तव्य ।
आप समझते होंगे
वह कौन-सा समय होता है
जब अन्धेरा
जीवन का
बीजशब्द बनता जाता है
हिंसक पशु
खुलेआम घूमा करते हैं ।
स्वर्णयुग
जो तुमने चाहे
मेरे लेखे
वह कठिन समय, वह बुरा समय ।
स्वर्णयुग के लिए
पीछे मत लौटो मेरे बच्चों
आगे बढ़ो
तुम्हारे बिना
कोई स्वर्णयुग होगा कैसे ?
तुम अपने भावी सपनों
का निर्माण करो
मायावी अतीत कारा है
इससे बाहर निकलो ।
इतना कह उस दिव्य-पुरुष ने
अपने बांए हाथ को झटका
सिगरेट
बुझ चुकी थी अब तक
जिसे उसने मसल कर फेंका ।
इससे पहले
कि उसके लम्बे वक्तव्य से
बाहर आ हम
कुछ कह पाते
वह काँपते हुए
एक प्रकाशवृत्त में बदला
और फिर गुम हो गया ।
चार पुरुष और स्वर्ण युगों पर शोकगीत-6
कई-कई दिनों के जागे
हम चारों जो विफल अभागे
निश्चिन्त हो कर सोए
बहुत दिनों तक खोए-खोए
भावी जीवन के स्वप्नों में
उठे तो फिर भूख के साथ ।
हम अपने समय से
खाए हुए लात
करना चाहें अब
नए दिनों की बात
मगर अब भी मुश्किलें बहुत थीं ।
गाँधी अब महज़
एक मजबूरी का नाम था
ब्रह्मचर्य-नहीं वर्य
नपुंसक बनाता जो
अहिंसा के नाम पर
कनपटी पर तमाचे
ऐसे में कौन अब
गाँधी को बाँचे ।
मजबूरी का नाम था
पूरा विचार ही
लाचार और बेकाम था ।
अब उसके नाम पर
डोलता नहीं पत्ता
घिस-घिस कर नाम उसका
चोंथ-नोच डाली सत्ता
ये बदलाव के दिन
अलबत्ता…।
शक्तिपात
समय आपात
संवैधानिक अधिकार ही
करते आघात ।
लोहिया और जयप्रकाश
अन्धकार में हारे
व्यर्थ हो चुके जैसे
चिन्तक सब लस्त-पस्त
सँगठित आन्दोलन
हुए पथभ्रष्ट न्यस्त ।
नक्सलबाड़ी के
शहीद मज़दूर-किसान
आत्महत्या को विवश नौजवान
अधूरे ही रहे ख़्वाब
हर बार हर सवाल
रह जाता लाजवाब ।
शासक और सन्त
एकमेक हो गए
करते हुए घोषणा —
इतिहास का अन्त
विचारों का अन्त
हा हन्त ! हा हन्त !
कपिता का अन्त
प्रभु-महन्त !
जब ईश्वर बौराया
जंगल-जंगल भटके
जब आतँकी हत्यारे
उसके पीछे दौड़ें
जब ईश्वर को भी
मुश्किल से जान बचानी हो
जब भक्तों ने ही
तख़्तों की हठ ठानी हो
वह कठिन समय, हमारा समय ।
चमकता हुआ बाज़ार
लपलपाते हुए हथियार
लील लेने को तैयार
समूचा संसार ।
मरता हुआ मेसोपोटामिया
घुटता हुआ कोरिया, ईरान
लातीन अमरीका, दक्षिण अफ्रीका
भूखा इथोपिया
क्यूबा, वियतनाम
ऐसे ही कितने नाम ।
अतीत से बाहर
हमारा वर्तमान कितना भयावना
साम्राज्यवादी कर
गहते केश
गिरवी होता जाता
हमारा प्यारा देश ।
स्पेशल इकानामिक जोन
लखटकिया कार
मोबाइल फ़ोन
चिन्ता से बाहर
आटा, किरासिन, नोन
स्पेशल इकनामिक जोन ।
किसान बेज़मीन
अपने स्वत्व से हीन
होकर माँगते-फिरते मुआवज़ा
भीख की तरह ।
भोगने को अभिशप्त सज़ा
लाठियाँ, हत्या, बलात्कार
व्यापक नरसँहार
और एक आतँककारी मौन
स्पेशल इकानामिक जोन ।
रक्तपात और लूट
देख-देख, टूट-टूट
फिर से एक बार जुड़े,
हम जैसे बहुत लोग
भागते-फिरते हैं छिपे
ऐसे ही लोगों की गही बाँह
हम चारों दोस्तों को
सूझी एक नई राह
हम चारों साथ मुड़े ।
चार पुरुष और स्वर्ण युगों पर शोकगीत-7
हम चार दोस्त
निकले वन की ओर ।
वन दरोगा की आँख बचाकर
एक गिरे पेड़ को
खींचकर लाए ।
बनाए उसे चीर कर चैले
फिर उपलों के ऊपर धरकर
चिता बनाई ।
चौराहे पर
सिनेमा के पोस्टर
चिपकाने के लिए
रखी हुई बाँस की सीढ़ी
को हमने लालच से देखा ।
उसकी डाण्ड़ों को तोड़
कर हमने
उसे मूँज से बाँधा
और टिकठी की शक्ल दी ।
हम चार पुरुषों ने
उस पर
लिटा दिए
अपने-अपने अतीत के स्वर्णयुग ।
हम चारों ने
अर्थी को अपने
पुनर्शक्तिसम्पन्न कन्धे दिए ।
हमने अपने स्वर्णयुगों की
चिता जलाई
अपने-अपने मोह
को राख होते हुए देखा ।
हम चार पुरुषों ने
हम चार दोस्तों ने
मृत स्वर्णयुगों पर
मिलकर गीत लिखा ।
मोहभंग से
ऊपर उठकर
मानो हँसते हुए स्वयँ पर
वह शोकगीत यहाँ
फिर से गा नहीं सकते ।
दिल्ली में एक दिन की राष्ट्रीय समस्या
दिल्ली हमारे देश की राजधानी है
इसलिए यहां की सरकारी समस्याएं राष्ट्रीय होती हैं
एक दिन समस्या यह थी कि एक प्रदेश के राज्यपाल को
उसके प्रदेश के राजभवन तक पहुंचाया कैसे जाए?
महामहिम पिछले कई दिनों से दिल्ली में थे
और सरकारी खर्च पर महंगा इलाज करा रहे थे
वे नींद में बड़बड़ाते थे कि देश में अच्छे डाक्टर नहीं
फिर भी अब वे पहले से स्वस्थ थे।
यह महाराजा के इलाज जैसी बात नहीं थी।
आमिर खान टेलीविजन पर महंगे इलाज और
महंगी दवाओं का अर्थशास्त्र समझा रहे थे
लेकिन मामला राज्यपाल का था और मुखिया के बिना
प्रदेश को नहीं छोड़ा जा सकता था बहुत दिनों तक
इसलिए उन्हें उनके राजभवन तक पहुंचाना ज़रूरी था
किसी संवैधानिक संकट उत्पन्न होने से पहले ही।
विकट राष्ट्रीय समस्या थी और
राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान सदैव राष्ट्रीय होते हैं।
हमारे देश में बिना वार्ताओं के समाधान नहीं निकला करते
इसलिए एक ही दिन में वार्ताओं के कई दौर चले
पहले उपसचिव स्तर की वार्ता हुई
फिर प्रदेश और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच
प्रमुख सचिव स्तर की वार्ता हुई
तब जा कर हेलीकॉप्टर से उन्हें ले जाना तय हुआ।
आयुर्विज्ञान संस्थान से निकल कर बीमार महामहिम ने
उड़ान भरी अपने प्रदेश के राजभवन की ओर
प्रशासन की जान में जान आयी और
प्रदेश को संवैधानिक संकट से बचाने की राष्ट्रीय समस्या
का राष्ट्रीय हल निकाल लिया गया था।
नरबलि : अभिधा की एक शाम
एक छोटी शाम जो
लम्बी खिंचती जाती थी
बिल्कुल अभिधा में ।
रक्ताभा लिए रवि
लुकता जाता था ।
लक्षणा के लद चुके
दिनों के बाद
व्यंजना की एक छोटी-सी शाम
धीरे-धीरे
करती रही अपना प्रसार
बढ़ती जाती थी भीड़
सिकुड़ रहा था सभागार ।
रचना ही बचना है
कोहराम मचना है ।
कहा कभी किसी ने
बेदाँत जबड़ों के बीच
कुतरे जाते हुए ।
अहंकार से लथपथ
शतपथी ब्राह्मणों के
पान से ललाये मुख
से होते हुए आख़िर
पेट में जो पचना है
आयताकार प्रकाश-पुंज
फैला है भीतर
बाहर शाम को
लील रहा अंधकार
मंच पर आसीन
पहने कौपीन
लदकर लिए घातक हथियार
आतुर थे करने को एकल संहार
वायु-मार्ग से आए
ऋषिगण करते आलोचन
लोहित-लोचन ।
थके चरण
वह वधस्थल को
जाता उन्मन, नतनयन
माला और दुशाला को
डाला एक कोने में;
वध के पश्चात रक्त
सहेज कर भगोने में,
तेज़ धार, वह कटार
पोंछ-पाछ, साफ़ कर
अन्तिम यह वाक्य कहा–
“हल्का है,
बासी है, कल का है,
डिम्ब है न बिम्ब है
अभिधा है, अभिधा है
अग्नि को जो अर्पण है
मेरी प्रिय समिधा है ।”.
निषाद-कन्या
मैं मछलियां बेचती हूँ
जल से ही शुरू हुआ जीवन
पृथ्वी पर, मेरा भी।
आदिकाल से ही अपने
देह की मत्स्यगंध लिए
महकती, डोलती
तुम्हारी वेगवती
कल्लोलिनी भाषा के प्रवाह में
मछलियां पकड़ती
अपने को खोलती।
मेरा ध्रुवतारा जल में है
मेरा चांद, मेरा सूरज
जल में ही दिपता है
मेरे लिए आरक्षित नहीं कुछ
मछली भर मेरी निजता है।
अपने गलफरों से सिर्फ़ तुम्हारे लिए
सांसे लेती थक गई हॅूं।
अपने घर लौट जाओ ऋषि!
तुम्हारे आत्मज संकल्पबद्ध हैं
और तुम्हारे पास
न अपनी जर्जर देह का कोई
विकल्प है, न परम्परा का।
ऋषि! लौट जाओ अपनी
अमरत्व और मोक्ष की
मोहक कामनाओं में।
मुझे तो इसी जल में
फिर-फिर जन्म लेना है।
पृथ्वी उदास है
एक दिन घूमते -घूमते
अचानक पृथ्वी उदास हो गयी
सहम गये ग्रह -उपग्रह -नक्षत्र सब
खगोलशास्त्रियों ने
टेलीस्कोप निकाले
और आसमान ताकते रहे
राष्ट्राध्यक्षों ने
राष्ट्रीय ध्वज झुका लिए
मगर पृथ्वी उदास रही
कवियों ने गीत लिखे
उदासमना पृथ्वी के लिए
चित्रकार उल्लसित पृथ्वी की
विभिन्न मुद्राएं बनाते रहे
नर्तकों ने घुंघरू पाँवों से उतारे
और शताब्दी को
नर शताब्दी की संज्ञा देते हुए
जी भर कर कोसा
फिर भी पृथ्वी उदास रही
पृथ्वी अब भी उदास है
कि राजा जनक के बाद
किसी किसान के हल का फल
किसी घड़े से
टकराया क्यों नहीं?
प्रतीक
भाषा में देश था
देश में धर्म
धर्म में नायक थे
नायकों में राम
राम में भय था
भय का पार्टी से लेकर
भेड़िये तक कई प्रतीक थे
प्रतीकों में प्रेम नहीं था
प्रेम का प्रतीक कोई नहीं था
बाबा और तानपूरा
निराला जी के पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी के लिए
घर के एक कोने में
खड़ा रहता था
बाबा का तानपूरा
एक कोने में
बाबा पड़े रहते थे
तानपूरा जैसे बाबा
बाबा पूरे तानपूरा
बुढ़ाते गए बाबा
बूढ़ा होता गया तानपूरा
झूलती गई बाबा की खाल
ढीले पड़ते गए
तानपूरे के तार
तानपूरे वाले बाबा
बाबा वाला तानपूरा
असहाय नहीं है
इनमें से कोई भी
बल्कि हमारी पीढ़ी में ही
कोई साधक नहीं हुआ