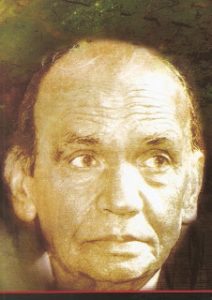
तबीयत में न जाने ख़ाम
बढ़ाता है तमन्ना आदमी आहिस्ता आहिस्ता
गुज़र जाती है सारी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता
अज़ल से सिलसिला ऐसा है गुंचे फूल बनते हैं
चटकती है चमन की हर कली आहिस्ता आहिस्ता
बहार-ए-जि़ंदगानी पर खज़ाँ चुपचाप आती है
हमें महसूस होती है कमी आहिस्ता आहिस्ता
सफ़र में बिजलियाँ हैं आँधियाँ हैं और तूफ़ाँ हैं
गुज़र जाता है उनसे आदमी आहिस्ता आहिस्ता
परेशाँ किसलिए होता है ऐ दिल बात रख अपनी
गुज़र जाती है अच्छी या बुरी आहिस्ता आहिस्ता
तबीयत में न जाने ख़ाम ऐसी कौन सी शै है
कि होती है मयस्सर पुख़्तगी आहिस्ता आहिस्ता
इरादों में बुलंदी हो तो नाकामी का ग़म अच्छा
कि पड़ जाती है फीकी हर खुशी आहिस्ता आहिस्ता
ये दुनिया ढूँढ़ लेती है निगाहें तेज़ हैं इसकी
तू कर पैदा हुनर में आज़री आहिस्ता आहिस्ता
तख़य्युल में बुलंदी औ’ ज़बाँ में सादगी ‘रहबर’
निखर आई है तेरी शायरी आहिस्ता आहिस्ता
बढ़ाता है तमन्ना आदमी आहिस्ता-आहिस्ता
बढ़ाता है तमन्ना आदमी आहिस्ता आहिस्ता,
गुज़र जाती है सारी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता ।
अज़ल से सिलसिला ऐसा है ग़ुंचे फूल बनते हैं,
चटकती है चमन की हर कली आहिस्ता आहिस्ता ।
बहार-ए-ज़िंदगानी परख़ज़ाँ चुपचाप आती है,
हमें महसूस होती है कमी आहिस्ता आहिस्ता ।
सफ़र में बिजलियाँ हैं, आंधियाँ हैं और तूफ़ाँ हैं,
गुज़र जाता है उनसे आदमी आहिस्ता आहिस्ता ।
हो कितनी शिद्दते-ए-ग़म वक़्त आख़िर पोंछ देता है,
हमारे दीदा-ए-तर[1] की नमी आहिस्ता आहिस्ता ।
परेशाँ किसलिए होता है ऐ दिल बात रख अपनी
गुज़र जाती है अच्छी या बुरी आहिस्ता आहिस्ता ।
तबियत में न जाने खाम ऐसी कौन सी शै है,
कि होती है मयस्सर पुख़्तगी आहिस्ता आहिस्ता ।
इरादों में बुलंदी हो तो नाकामी का ग़म अच्छा,
कि पड़ जाती है फीकी हर ख़ुशी आहिस्ता आहिस्ता ।
छुपाएगी हक़ीक़त को नमूद-ए-जाहिरी[2] कब तक,
उभरती है शफ़क[3] से रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ।
ये दुनिया ढूँढ़ लेती है निगाहें तेज़ हैं इसकी
तू कर पैदा हुनर में आज़री[4] आहिस्ता आहिस्ता ।
तख़य्युल[5] में बुलन्दी और ज़बाँ में सादगी ‘रहबर’
निखर आई है तेरी शायरी आहिस्ता आहिस्ता ।
रचनाकाल : 16 नवम्बर 1941, सेंट्रल जेल, संगरूर
चाँदनी रात है जवानी भी
चाँदनी रात है जवानी भी,
कैफ़ परवर भी और सुहानी भी ।
हल्का-हल्का सरूर रहता है,
ऐश है ऐश ज़िन्दगानी भी ।
दिल किसी का हुआ, कोई दिल का,
मुख्तसर-सी है यह कहानी भी ।
दिल में उलफ़त, निगाह में शिकवे
लुत्फ़ देती है बदगुमानी भी ।
बारहा बैठकर सुना चुपचाप,
एक नग़मा है बेज़बानी भी ।
बुत-परस्ती की जो नहीं कायल
क्या जवानी है वो जवानी भी ।
इश्क़ बदनाम क्यों हुआ ‘रहबर
कोई सुनता नहीं कहानी भी ।
रचनाकाल : 15 नवम्बर 1941, सेंट्रल जेल, संगरूर
उसका भरोसा क्या यारो वो शब्दों का व्यापारी है
उसका भरोसा क्या यारो वो शब्दों का व्यापारी है,
क्यों मुँह का मीठा वो न हो जब पेशा ही बटमारी है ।
रूप कोई भी भर लेता है पाँचों घी में रखने को,
तू इसको होशियारी कहता लोग कहें अय्यारी है ।
जनता को जो भीड़ बताते मँझधार में डबेंगे,
काग़ज़ की है नैया उनकी शोहरत भी अख़बारी है ।
सुनकर चुप हो जाने वाले बात की तह तक पहुँचे हैं,
कौवे को कौवा नहीं कहते यह उनकी लाचारी है ।
पेड़ के पत्ते गिनने वालो तुम ‘रहबर’ को क्या जानो,
कपड़ा-लत्ता जैसा भी हो बात तो उसकी भारी है ।
रचनाकाल : 11 अप्रैल 1976, सेंट्रल जेल, तिहाड़, दिल्ली
किस कदर गर्म है हवा देखो
किस कदर गर्म है हवा देखो,
जिस्म मौसम का तप रहा देखो ।
बदगुमानी-सी बदगुमानी है,
पास होकर भी फ़ासला देखो ।
वे जो उजले लिबास वाले हैं,
उनकी आँखों में अज़दहा[1] देखो ।
हो अंधेरा सफ़र, सफ़र ठहरा,
ले के चलते हैं हम दिया देखो ।
खेलता है जो मौत से होली,
क्या करेगा वो मनचला देखो ।
अम्न ही अम्न सुन लिया, लेकिन,
मक़तलों का भी सिलसिला देखो ।
इस ज़माने में जी लिया ‘रहबर’
मर्दे-मोमिन[2] का हौसला देखो ।
रचनाकाल : 01 मई 1980, दिल्ली
शब्दों का व्यापारी
उसका भरोसा क्या यारों, वो शब्दों का व्यापारी है,
क्यों मुँह का मीठा वो न हो, जब पेशा ही बटमारी है।
रूप कोई भी धर लेता है पाँचों घी में रखने को,
तू इसको होशियारी कहता, लोग कहें अय्यारी है।
जनता को जो भीड़ बताते मँझधार में डूबेंगे,
काग़ज़ की है नैया, उनकी शोहरत भी अख़बारी है।
सुनकर चुप हो जाने वाले बात की तह तक पहुँचे हैं,
कौवे को कौवा नहीं कहते, यह उनकी लाचारी है।
पेड़ के पत्ते गिनने वालो तुम ‘रहबर’ को क्या जानो,
कपड़ा-लत्ता जैसा भी हो, बात तो उसकी भारी है।
रचनाकाल : 11 अप्रैल 1976, तिहाड़ जेल